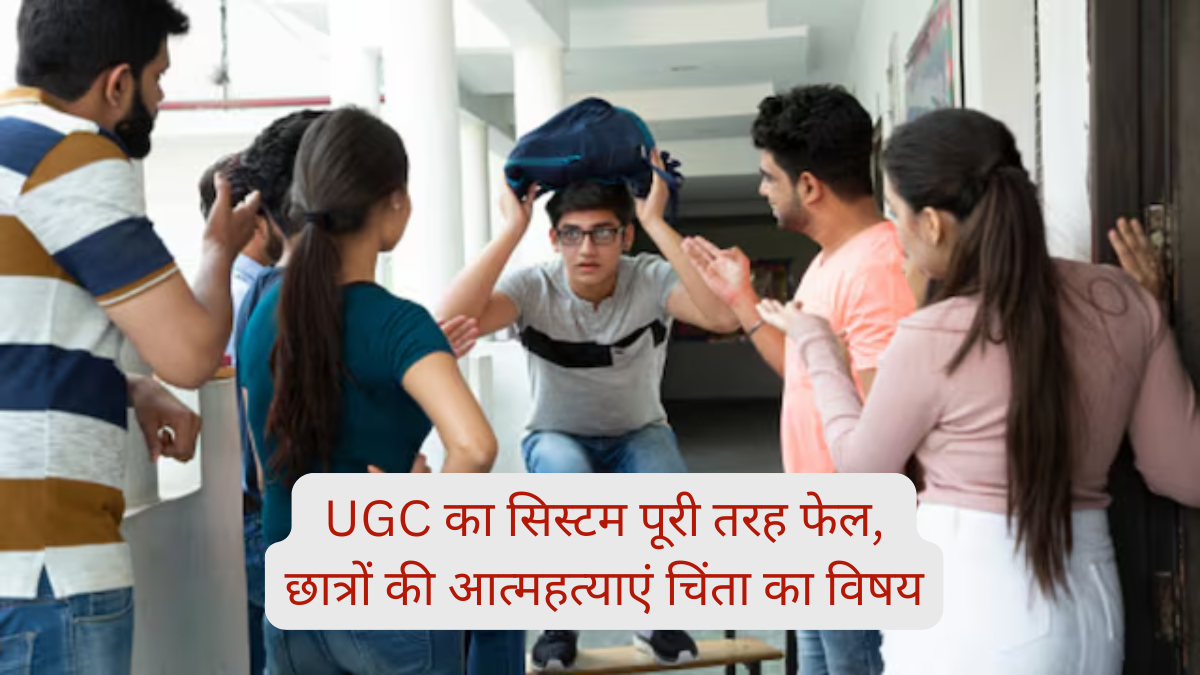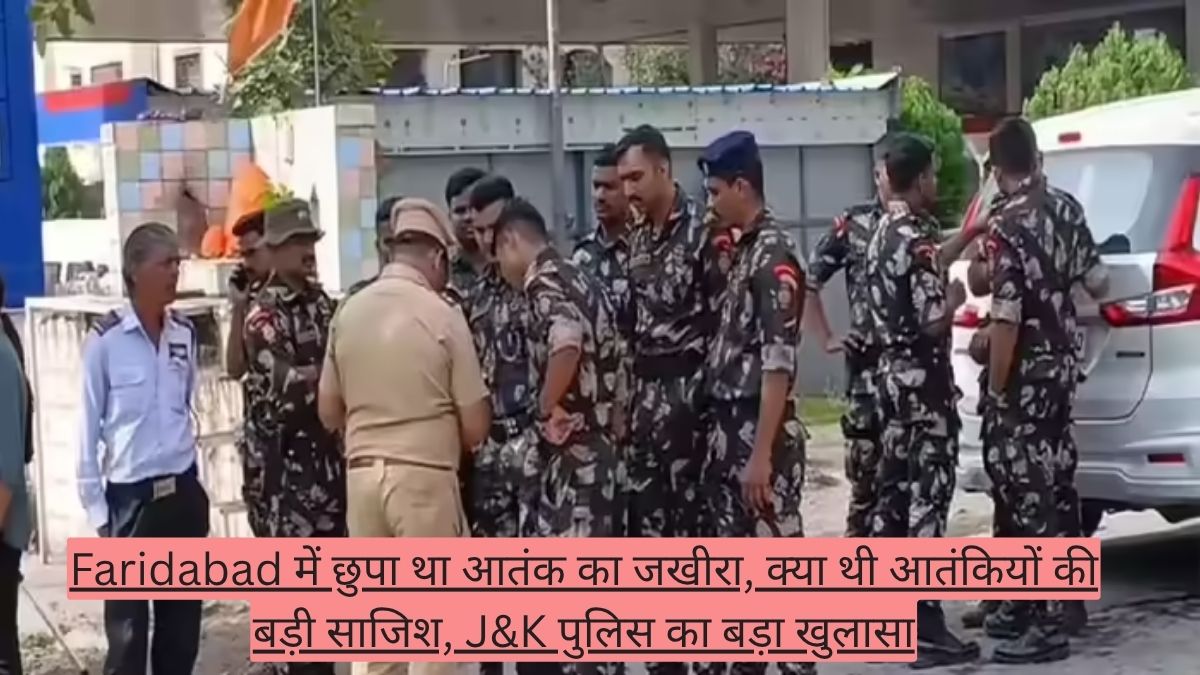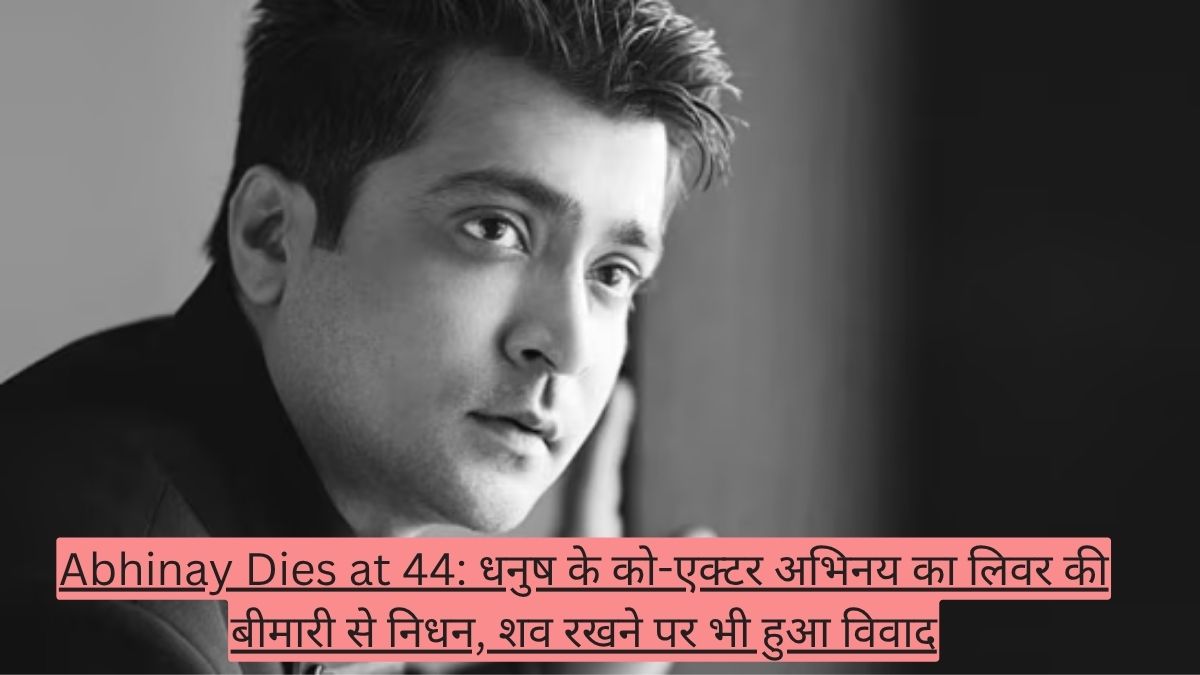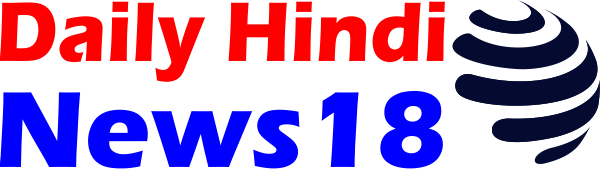भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions) में रैगिंग (Ragging) एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो आए दिन छात्रों की जान लेने या उन्हें मानसिक पीड़ा देने का कारण बन रही है। कड़े नियमों और ‘शून्य सहनशीलता’ (Zero Tolerance) की नीति के बावजूद, देश भर के भारतीय कैंपसों (Indian Campuses) में यह कुप्रथा अभी भी पनप रही है। इस गंभीर मुद्दे को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गंभीरता से लिया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के एंटी-रैगिंग सिस्टम (Anti-Ragging System) की पूर्ण विफलता पर कड़ी फटकार लगाई है। छात्रों द्वारा बढ़ती आत्महत्याओं (Student Suicides) और शिकायतों की संख्या से आहत अदालत ने संकेत दिया है कि वह लोकहित याचिका (PIL) के माध्यम से इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने UGC के एंटी-रैगिंग सिस्टम को क्यों आड़े हाथों लिया?
यूजीसी (UGC) भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग विरोधी नीतियों को बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, हालिया आंकड़ों ने इसकी प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 के बीच, UGC की एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर 1,240 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो लगभग एक दशक में सबसे अधिक संख्या है। यह डेटा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समस्या बढ़ रही है।
चिंताजनक आंकड़े: छात्रों की आत्महत्याएं और रैगिंग का संबंध:
2022 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के अनुसार, एक ही वर्ष में 13,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा भारत में सभी आत्महत्या मौतों का 7.6% है, जो किसानों और कृषि मजदूरों की संयुक्त आत्महत्याओं से भी अधिक है। हालाँकि इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर रैगिंग को कारण के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कई मामलों में रैगिंग के कारण होने वाला मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।
कागजों पर ‘शून्य सहनशीलता’: हकीकत क्या है?
UGC की वर्तमान एंटी-रैगिंग नीति 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्देश (Supreme Court Directive) के बाद बनाई गई थी। सैद्धांतिक रूप से, इसमें वे सभी आवश्यक तत्व शामिल हैं जो एक प्रभावी प्रणाली के लिए ज़रूरी हैं:
- 24×7 हेल्पलाइन: 1800-180-5522
- समर्पित पोर्टल: www.antiragging.in
- छात्रों और अभिभावकों से अनिवार्य हलफनामा (Affidavits)
- सभी कॉलेजों में अनिवार्य एंटी-रैगिंग समितियाँ
- आकस्मिक निरीक्षण (Surprise Inspections), जागरूकता पोस्टर (Awareness Posters), और सख्त कार्रवाई दिशानिर्देश
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में रैगिंग को दंडनीय अपराध के रूप में माना गया है, जिसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ली है। यद्यपि BNS रैगिंग को एक अलग अपराध के रूप में विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है, यह ऐसे प्रावधानों को बनाए रखता है जो विशिष्ट रैगिंग-संबंधित कृत्यों को आपराधिक बनाते हैं। अपराध की गंभीरता के आधार पर, दोषियों पर आपराधिक धमकी (Section 351), गलत तरीके से रोकना (Wrongful Restraint – Section 337), अश्लील कृत्य (Obscene Acts – Section 294) और अत्यधिक गंभीर मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाना (Abetment of Suicide – Section 108) या हत्या के बराबर गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide not amounting to Murder – Section 105) जैसी धाराओं के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान UGC के समर्पित एंटी-रैगिंग नियमों (2009) और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के साथ संचालित होते हैं।
धरातल पर प्रभाव नगण्य: ऑडिट का खुलासा:
सेंटर फॉर यूथ (C4Y) द्वारा 2023 के एक ऑडिट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 60% कॉलेजों में एंटी-रैगिंग समितियाँ या तो कार्यात्मक नहीं थीं या केवल कागजों पर मौजूद थीं। यह दर्शाता है कि कानून के होने के बावजूद, उनका प्रवर्तन (Enforcement) बेहद कमजोर है। UGC का खंड 9.4 (Clause 9.4) नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के लिए धन कटौती की अनुमति देता है, लेकिन इसे शायद ही कभी लागू किया गया हो। 2023-24 UGC डेटा के अनुसार, केवल 10% रैगिंग शिकायतों पर ही FIR दर्ज हुईं।
रैगिंग क्यों जारी है: हकीकत का सामना
कड़े कानून और सार्वजनिक अभियानों के बावजूद, रैगिंग भारतीय कॉलेज संस्कृति (Indian College Culture) में गहरी जड़ें जमाए हुए है। इसके कई कारण हैं:
- खराब प्रवर्तन (Poor Enforcement): अधिकांश कॉलेज एंटी-रैगिंग उपायों को केवल औपचारिकता मानते हैं। आकस्मिक निरीक्षण शायद ही कभी होते हैं, और समितियों की बैठकें ज्यादातर कागजों पर ही सिमट जाती हैं।
- सत्ता की गतिशीलता और ‘परंपरा’ (Power Dynamics & ‘Tradition’): रैगिंग को अक्सर ‘स्वागत संस्कार’ (Welcome Ritual) या ‘बॉन्डिंग एक्सरसाइज’ (Bonding Exercise) के रूप में पेश किया जाता है, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में। यह अक्सर सीनियर्स द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका होता है। ये विषाक्त परंपराएं (Toxic Traditions) संस्कृति के आड़ में अनियंत्रित रहती हैं।
- प्रतिशोध का डर (Fear of Retaliation): अधिकांश पीड़ित चुप रह जाते हैं क्योंकि वे सीनियरों द्वारा उत्पीड़न, सामाजिक अलगाव (Social Isolation), या कमजोर करार दिए जाने के डर से ग्रस्त होते हैं। SAVE (Society Against Violence in Education) के 2020 के एक अध्ययन में पाया गया कि रैगिंग का सामना करने वाले केवल 8.6% छात्रों ने ही इसकी रिपोर्ट की थी।
- जागरूकता की कमी (No Real Awareness): नए छात्रों (Freshers) को यह भी नहीं पता होता कि शिकायत कैसे दर्ज करनी है। ओरिएंटेशन सत्रों (Orientation Sessions) में अक्सर यह जानकारी छोड़ दी जाती है, और एंटी-रैगिंग पोस्टर, यदि लगे भी हों, तो आसानी से नज़रअंदाज़ हो जाते हैं। जिन छात्रों को सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें यह नहीं पता कि मदद कहाँ से मिलेगी।
- कॉलेज अपनी छवि की रक्षा करते हैं: कई संस्थान खराब प्रचार (Bad Press) या जांच से बचने के लिए शिकायतों को दबा देते हैं (Bury Complaints)। 2007 के एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित राघवन समिति (Raghavan Committee) ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि कॉलेज अक्सर पीड़ितों को दरकिनार कर देते हैं और कानून प्रवर्तन को शामिल करने से बचते हैं।
आंकड़े चीख-चीख कर कह रहे हैं:
- हेल्पलाइन शिकायतों में 582 (2021-22) से बढ़कर 1,240 (जनवरी 2023–अप्रैल 2024) हो गई हैं – यह 45% की वृद्धि है।
- मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज (Medical and Engineering Colleges) देश भर में रैगिंग के 40% मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।
- छात्र आत्महत्याएं: 2022 में महाराष्ट्र (1,764), तमिलनाडु (1,416), मध्य प्रदेश (1,340)।
- रैगिंग से जुड़ी मौतें: 2012–2023 के बीच 78 मौतें – जो पहले प्रति वर्ष औसतन 7 थीं, वे 2022 के बाद प्रति वर्ष 17 तक बढ़ गई हैं।
- यद्यपि UGC ने 2023-24 में 90% मामलों को बंद कर दिया, लेकिन अधिकांश मामलों को हल्की सजाओं के साथ आंतरिक रूप से निपटाया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट की चेतावनी का मतलब:
अदालत की “यह सिस्टम पूरी तरह विफल रहा है” जैसी कड़ी टिप्पणी ASKT की उस याचिका के जवाब में आई थी, जिसने रैगिंग से जुड़ी छात्र आत्महत्याओं पर प्रकाश डाला था। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो वह खुद इस मुद्दे को उठा सकती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि न्यायपालिका UGC की खोखली बातों (Lip Service) से अपना धैर्य खो रही है। इसके परिणामस्वरूप तीसरे पक्ष के ऑडिट (Third-party Audits), कार्रवाई के लिए सख्त समय-सीमा, या छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने वाले संस्थानों पर जुर्माना जैसे नए सुधार हो सकते हैं।
अन्य देशों से सीखें: रैगिंग से निपटने के बेहतर तरीके
दुनिया भर में रैगिंग (या हेजिंग – Hazing) मौजूद है, लेकिन कई देशों ने इससे बेहतर तरीके से निपटने के तरीके खोजे हैं:
- संयुक्त राज्य अमेरिका (US): विश्वविद्यालय कड़े एंटी-हेजिंग कानूनों (Strict Anti-hazing Laws) का पालन करते हैं। कैलिफोर्निया का मैट्स लॉ (Matt’s Law), यदि हेजिंग से नुकसान होता है, तो जेल का प्रावधान करता है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK): छात्र संघ पीयर-टू-पीयर एंटी-बुलिंग (Peer-to-Peer Anti-Bullying) प्रयासों का नेतृत्व करते हैं। शिकायत दर्ज करना आसान है, और प्रतिशोध (Retaliation) दुर्लभ है।
- ऑस्ट्रेलिया (Australia): गुमनाम पोर्टल (Anonymous Portals), अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण (Mandatory Online Training), और त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई (Quick Disciplinary Action) एक बड़ा बदलाव लाते हैं।
भारत में कहाँ सुधार की आवश्यकता है:
भारत में, केंद्रीय UGC-संचालित प्रणाली (Centralised UGC-driven system) काफी हद तक संस्थागत अनुपालन (Institutional Compliance) पर निर्भर करती है। रिपोर्टिंग का डर और छात्र-आधारित सुरक्षा नेटवर्क (Student-led Safety Networks) की कमी स्थिति को और खराब बनाती है।
रैगिंग इसलिए पनपती है क्योंकि सिस्टम इसे पनपने देता है। जब कानून लागू नहीं होते और पीड़ित चुप रहते हैं, तो ‘शून्य सहनशीलता’ एक खोखला नारा बन जाता है। ‘शून्य सहनशीलता’ को नारे से अधिक बनाने के लिए, निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
- वास्तविक जागरूकता (Real Awareness): नए छात्रों को केवल हेल्पलाइन का उल्लेख करने से अधिक की आवश्यकता है। बहुभाषी पोस्टर (Multilingual Posters), व्हाट्सएप-आधारित अपडेट (WhatsApp-based Updates), और छात्र-नेतृत्व वाली ओरिएंटेशन वार्ता (Student-led Orientation Talks) एक लंबा रास्ता तय कर सकती हैं।
- कठोर परिणाम (Strict Consequences): UGC को अपने नियमों का पालन करना चाहिए – उन कॉलेजों को धन से वंचित करना चाहिए या उनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए जो एंटी-रैगिंग जनादेश (Anti-ragging Mandates) की अनदेखी करते हैं। हिंसक मामलों में तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए।
- स्वतंत्र निरीक्षण (Independent Oversight): निष्पक्ष निकायों द्वारा वार्षिक ऑडिट में हर कॉलेज के एंटी-रैगिंग सेटअप का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, यह जांचना चाहिए कि क्या समितियाँ वास्तव में मिलती हैं, और क्या रिपोर्टों पर कार्रवाई की जाती है।
- गुमनाम रिपोर्टिंग (Anonymous Reporting): हेल्पलाइन को एक तेज, अधिक गुमनाम प्लेटफॉर्म में अपग्रेड किया जाना चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार स्थानीय पुलिस तक सीधी पहुँच हो। कार्रवाई में देरी से विश्वास कम होता है।
परिवर्तनकारी कदम और सांस्कृतिक बदलाव:
कैम्पस संस्कृति में बदलाव (Campus Culture Shift) भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यशालाएं (Workshops), छात्र क्लब (Student Clubs), और मेंटरशिप समूह (Mentorship Groups) को सक्रिय रूप से जุนियर-सीनियर गतिशीलता को चुनौती देनी चाहिए। शिक्षकों (Faculty) और प्रशासनिक कर्मचारियों (Admin Staff) को भी पीड़ितों के प्रति अधिक संवेदनशील होने और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली हाईकोर्ट की इस कड़ी फटकार के बाद, UGC और संबंधित प्राधिकरण रैगिंग के खिलाफ लड़ाई को गंभीरता से लेंगे और उन प्रभावी उपायों को लागू करेंगे जो छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें।